(डॉ. सुधाकर आशावादी-विनायक फीचर्स)
किसी की राष्ट्र की समृद्धि नागरिकों के सकारात्मक चिंतन एवं राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों के समर्पित निर्वहन से होती है। नागरिक कर्तव्य सिखाए नहीं जाते, ये आत्मबोध का विषय होते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में जहां आम जन के रीति रिवाजों और जीवन शैली में अंतर है तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ भी भिन्न हैं, वहां सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सामूहिक प्रयास अपेक्षित हैं। साथ ही कुछ ऐसे बिंदुओं पर आम नागरिकों का राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है, जिनसे राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ किया जा सके। यह पांच सूत्र हैं – सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन , पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य। इन मुद्दों पर यदि किसी संस्थागत, व्यक्तिगत, दलगत, क्षेत्रवाद व भाषावाद के विचार से ऊपर उठकर चिंतन किया जाए तथा इनको अपने आचरण में समाहित करते हुए सृजनात्मक प्रयास किए जाएं, तो अवश्य ही भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
भारत की समृद्धि के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समृद्धि तक सीमित न रहते हुए यदि व्यवहारिक रूप से पंच परिवर्तन हेतु आम नागरिक स्वयं को समर्पित करे, तो अवश्य ही देश में उत्पन्न की गई अनेक समस्याओं का स्वतः निदान हो जाएगा। इस संदर्भ में व्यापक चर्चा करें तो स्पष्ट होगा, कि स्वाधीनता के उपरांत से जिस प्रकार राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ राजनीतिक दलों व के अलम्बरदारों द्वारा समाज को जातियों तक सीमित करके ऊँच नीच, दलित सवर्ण, अगड़ा पिछड़ा, की खाई चौड़ी करके राष्ट्र की जगह जाति, धर्म, क्षेत्र भाषा के नाम पर अलगाव उत्पन्न किया गया, उस अलगाव को सामाजिक समरसता से मिटाया जा सकता है। बरसों से जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए एक संस्था सक्रिय है, जो समूह भोज के माध्यम से सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। कुछ पंथ हैं, जो समाज में कर्म आधारित व्यवस्था के पक्षधर हैं तथा मानवता के प्रति समर्पित हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज इस क्षेत्र में डेढ़ शताब्दी से जुटा है। सिख पंथ की मानव सेवा सामाजिक समरसता का मानक है। अन्य अनेक ऐसे पंथ हैं, जो सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए पूर्ण समर्पित हैं।
दूसरा परिवर्तन बिंदु है – कुटुंब प्रबोधन। इस सन्दर्भ में अपनी साझा संस्कृति एवं समृद्ध पारिवारिक परंपराओं का स्मरण करना अनिवार्य है, कि समाज की पहली इकाई परिवार होता है। परिवार से ही संस्कार प्राप्त होते हैं तथा सेवा, सहयोग, समर्पण व आज्ञाकारिता जैसे मूल्य बालक में विकसित होते हैं, जो राष्ट्र के सकारात्मक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यदि समाज की पहली इकाई को सशक्त किया जाए तथा भौतिक सुख सुविधाओं के आधार पर जीवन यापन के लिए अपनाए जाने वाले एकल परिवार की विचारधारा पर गंभीर चिंतन किया जाए, तो पुनः कुटुंब की व्यवस्था के अनुपालन से पारिवारिक समृद्धि तो होगी ही साथ ही पारिवारिक सुरक्षा का भाव भी प्रत्येक के मन में जागृत रहेगा। आत्मरक्षा का भाव जो समूह में अधिक आत्मविश्वास जगाता है, वह एकल परिवार में कभी भी नहीं पनप सकता। सो अपनी पारिवारिक जड़ों से जुड़कर रहना समय की मांग है।
तीसरा परिवर्तन बिंदु है – पर्यावरण संरक्षण। कौन नहीं जानता, कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचारों को जन्म देता है। शुद्ध पर्यावरण के अभाव में जीवन यापन सरल नहीं है। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ आवास उत्तम पर्यावरण से ही उपलब्ध हो सकते हैं। जिसके लिए समूचे समाज के लिए आवश्यक है कि वह पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचें। अपने ही हाथों विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से पर्यावरण को दूषित न करें। देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में अत्यधिक प्रदूषण से जानलेवा बीमारियों का बोलबाला रहता है। कहीं वायु प्रदूषण है तो कहीं जल प्रदूषण हैं। धार्मिक व पारिवारिक उत्सवों में ध्वनि प्रदूषण भी बच्चों व बीमार बुजुर्गों के लिए जानलेवा बन रहा है। ऐसे में यदि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक न हुए, तब अपने ही हाथों समय से पहले जान गंवाने हेतु विवश होना पड़ सकता है।
पंच परिवर्तन की दिशा में चौथा तथा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वदेशी आचरण। यूँ तो मौलिक आचरण स्वदेशी ही होता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसे अपने देश या अपनी संस्कृति से प्यार न हो। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सकारात्मक प्रयोग करते हुए आत्मनिर्भर बनें। जिन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में हो सकता है, उन वस्तुओं का आयात करने से परहेज करें तथा अपने देश के उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ हों। भौतिकवाद के आकर्षण में फंसकर अनुपयोगी वस्तुओं में धन व्यय न करें। स्वदेशी संसाधनों के प्रति जन जन का विशेष लगाव बना रहे। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग हेतु सभी नागरिक संकल्पबद्ध हों। स्वाधीनता के उपरांत भारत में जब कृषि संसाधनों का अभाव था. एक समय ऐसा भी आया कि जब कृषि प्रधान देश को विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ा तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सप्ताह में एक बार भोजन न करने का आह्वान किया तथा स्वयं भी यह संकल्प धारण किया। इसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत हेतु श्री मोहन दास कर्म चंद गाँधी ने घरेलू कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दैनिक प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का निर्माण करने हेतु गाँधी आश्रम जैसी स्वदेशी विचारधारा देश को सौंपी। स्वरोजगार, स्वदेशी का भाव आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना,जिसके प्रति आज भी समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है।
पंच परिवर्तन अवधारणा का अंतिम एवं पांचवां सूत्र है – नागरिक कर्तव्य। सच तो यह है कि जब तक देश का आम नागरिक अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने नागरिक अधिकारों का अनुपालन नहीं करेगा, तब तक प्रथम चारों सूत्र पूर्ण नहीं होंगे। राष्ट्र सामूहिक प्रयासों तथा नागरिकों के राष्ट्र के प्रति समर्पित आचरण से ही समृद्ध होता है। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक का अपने परिवार, जाति और धर्म के प्रति समर्पण से ऊपर उठकर प्रथम समर्पण राष्ट्र के प्रति हो। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण एवं संवर्धन में उसकी भागीदारी हो। सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव, सार्वजनिक स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आम नागरिक का कर्तव्य सहयोगी की भूमिका निभाना हो. राष्ट्रीय अनुशासन हेतु जन सुरक्षा के प्रति भी वह जागरूक बने। सार्वजनिक स्थलों पर जल, अन्न की बर्बादी रोकने में श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका का निर्वहन करें। स्वयं तो नागरिक कर्तव्य निभाए ही, औरों को भी नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित करें। *(विनायक फीचर्स)*

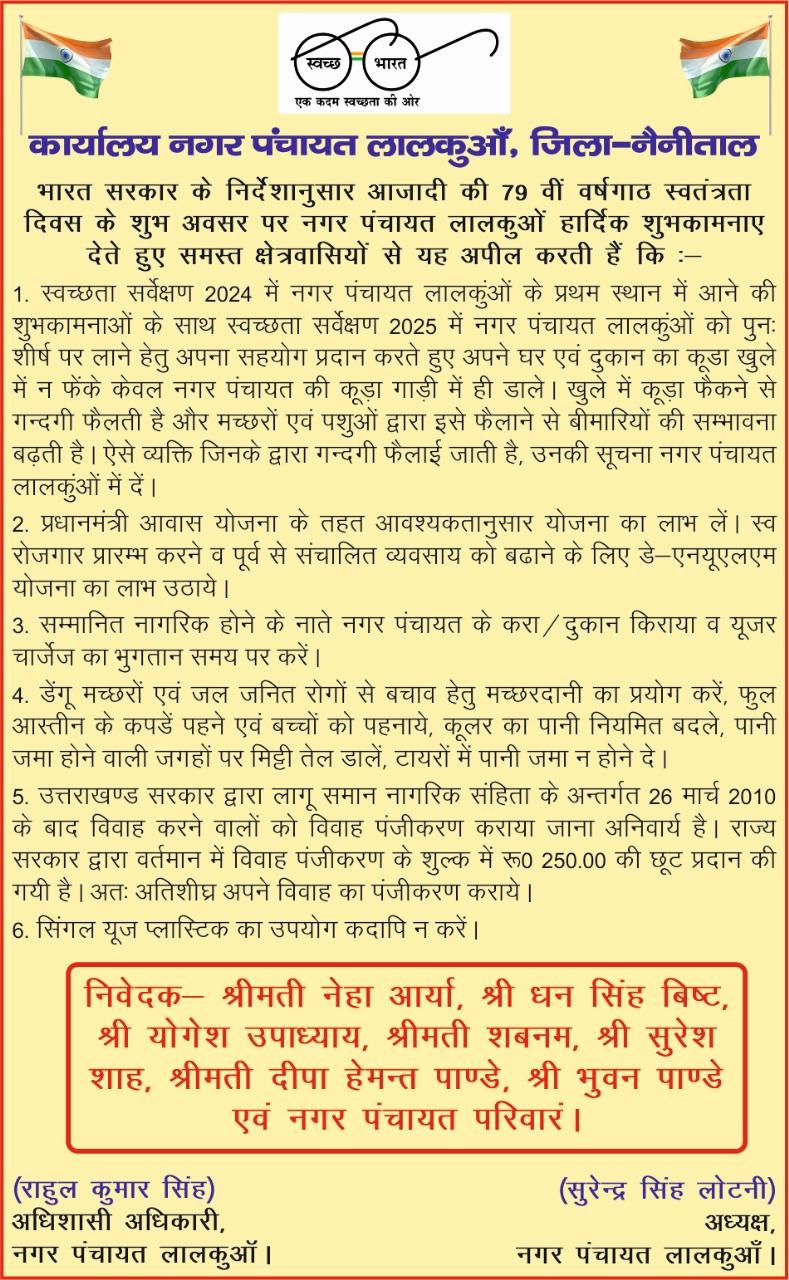
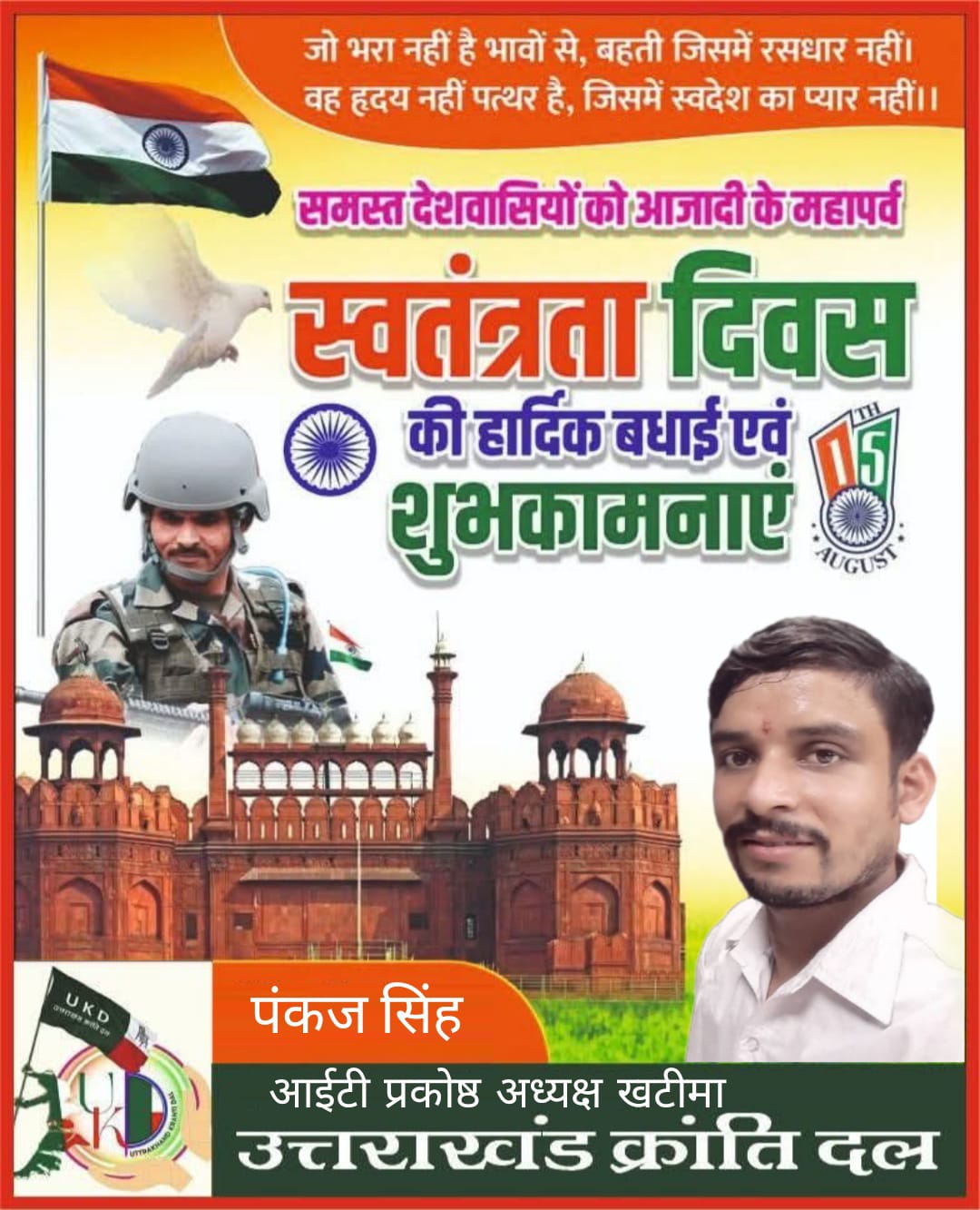
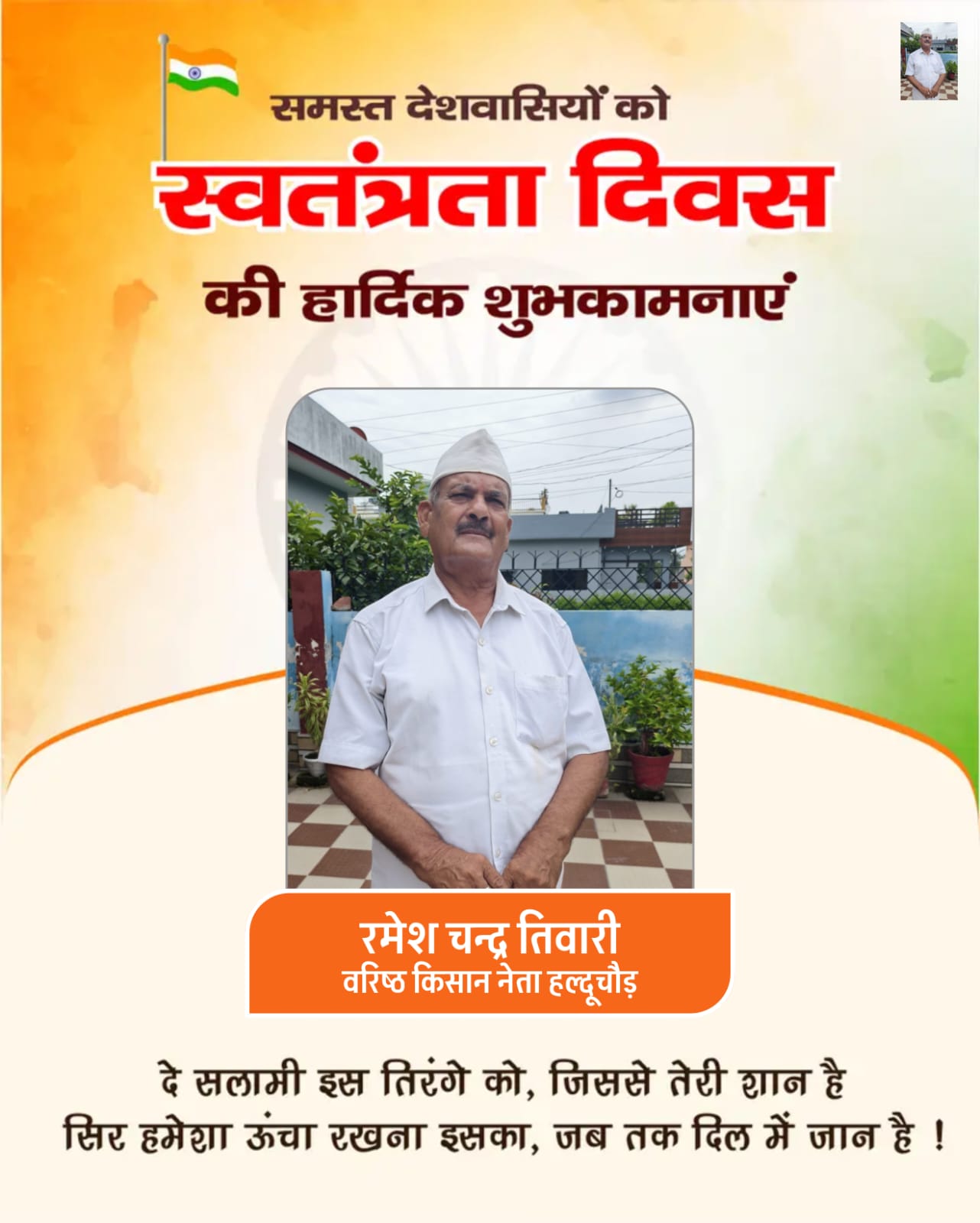
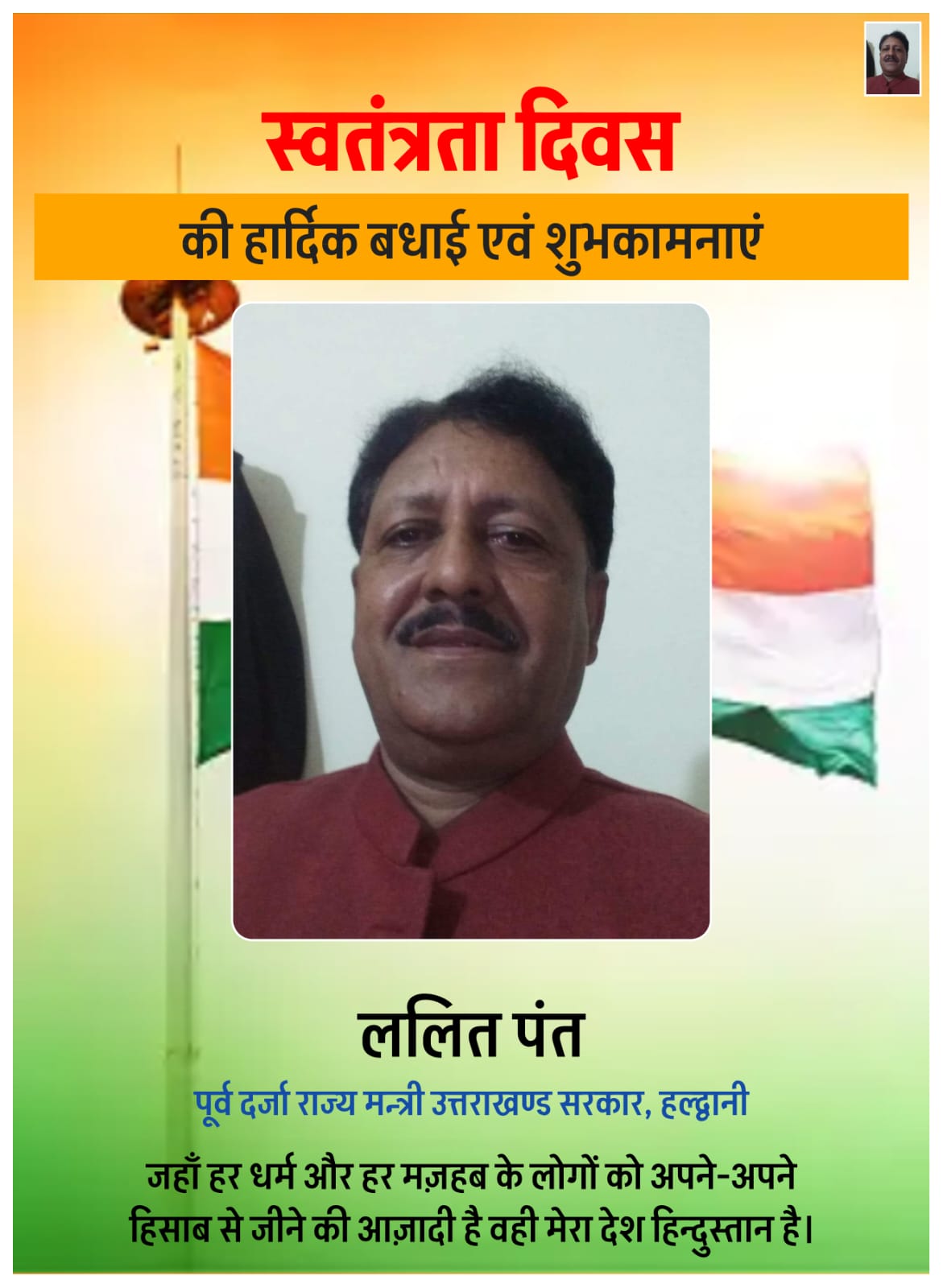
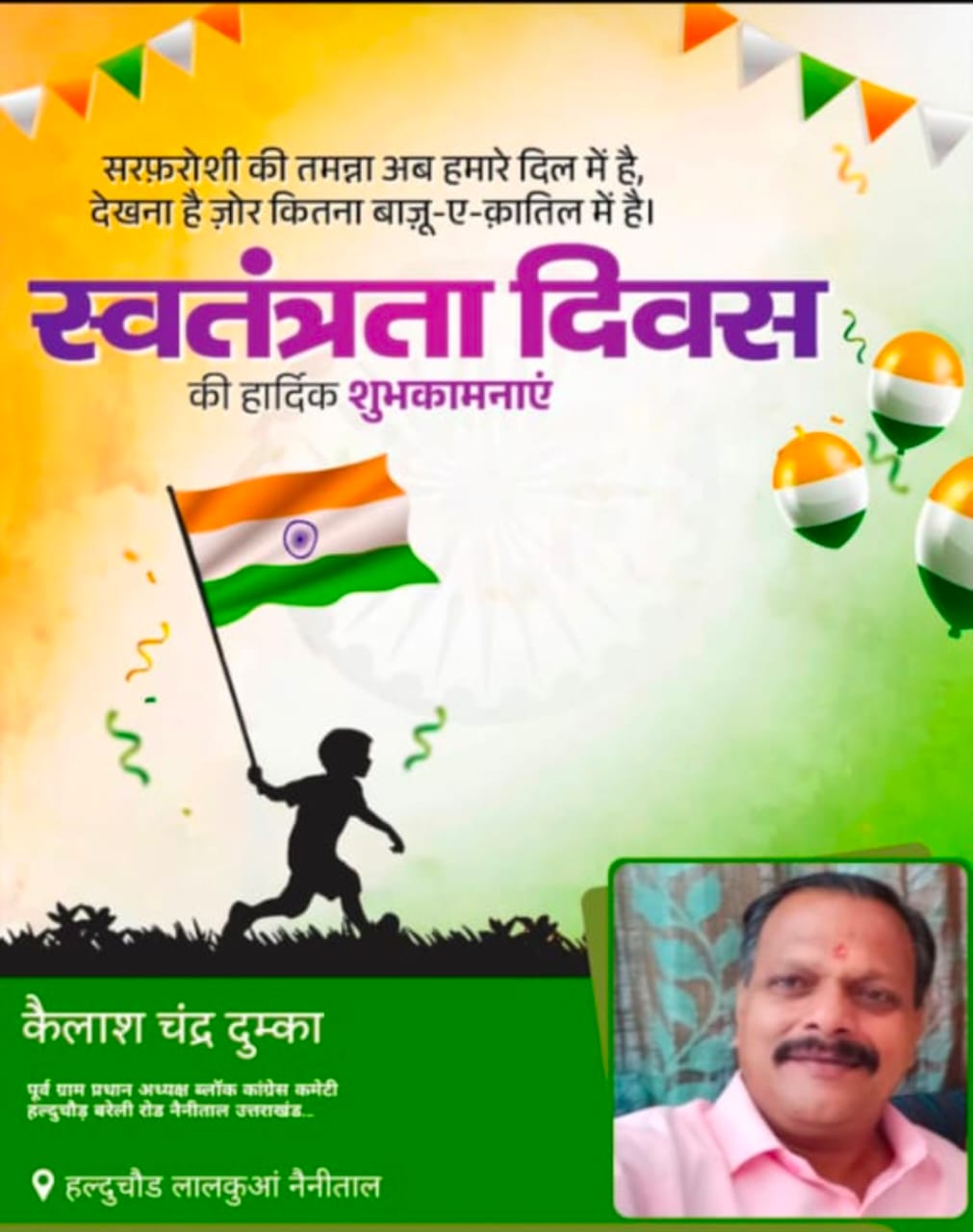
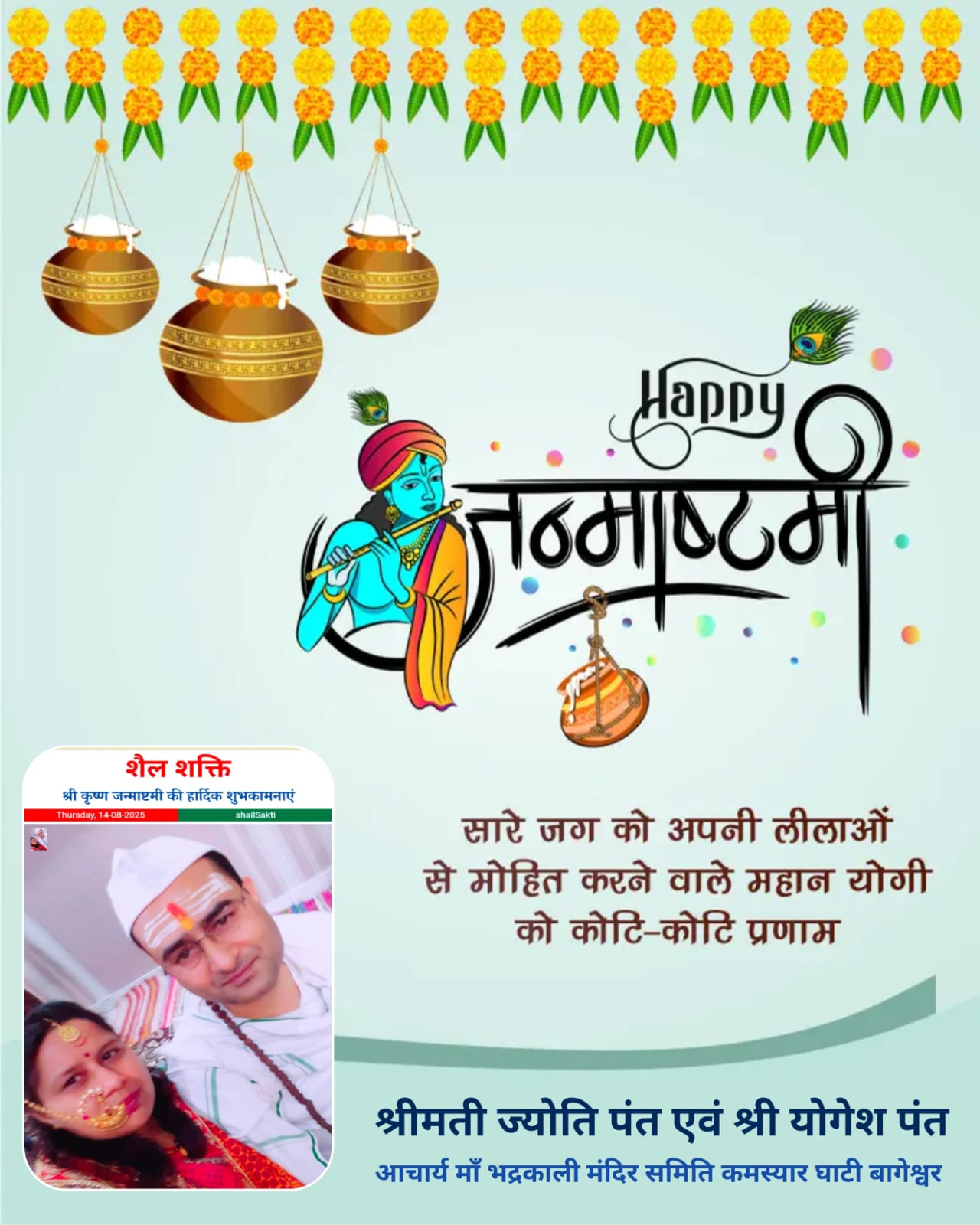
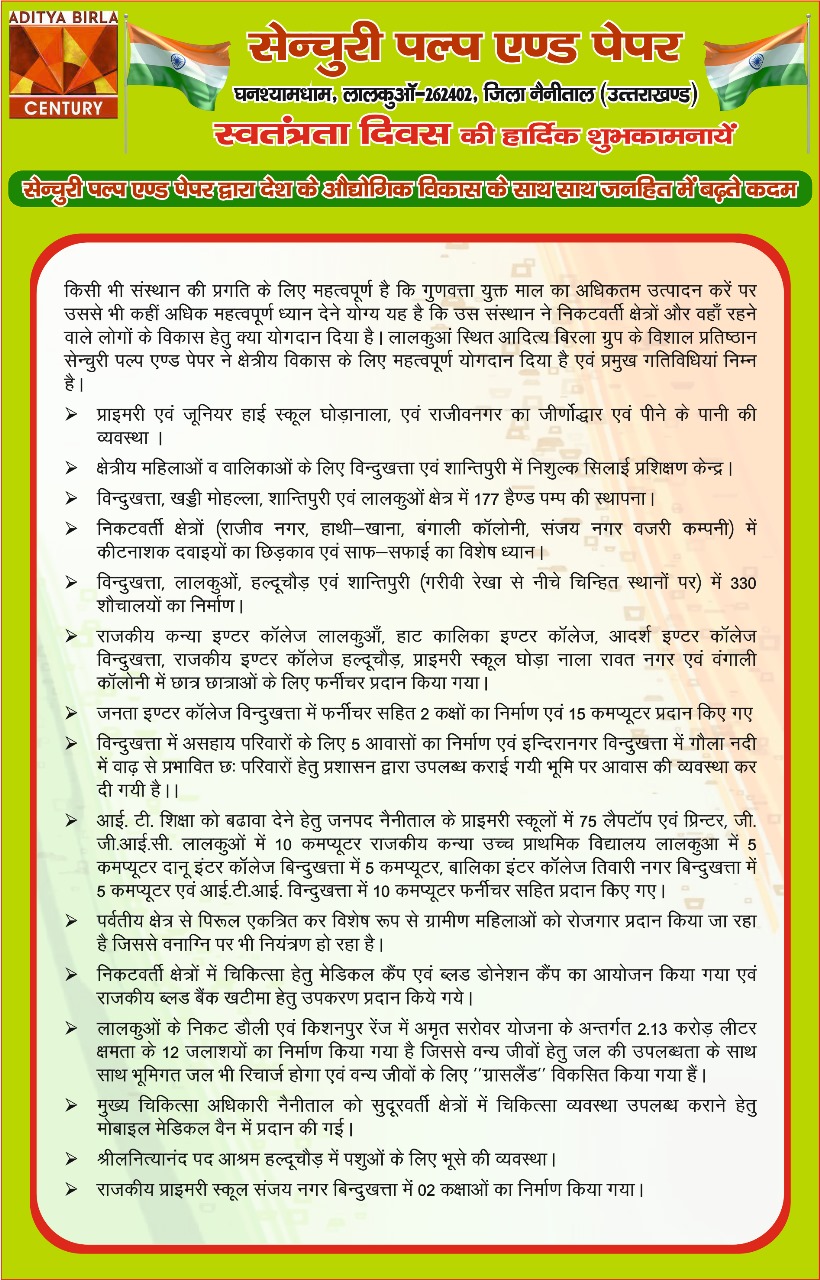



लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें

