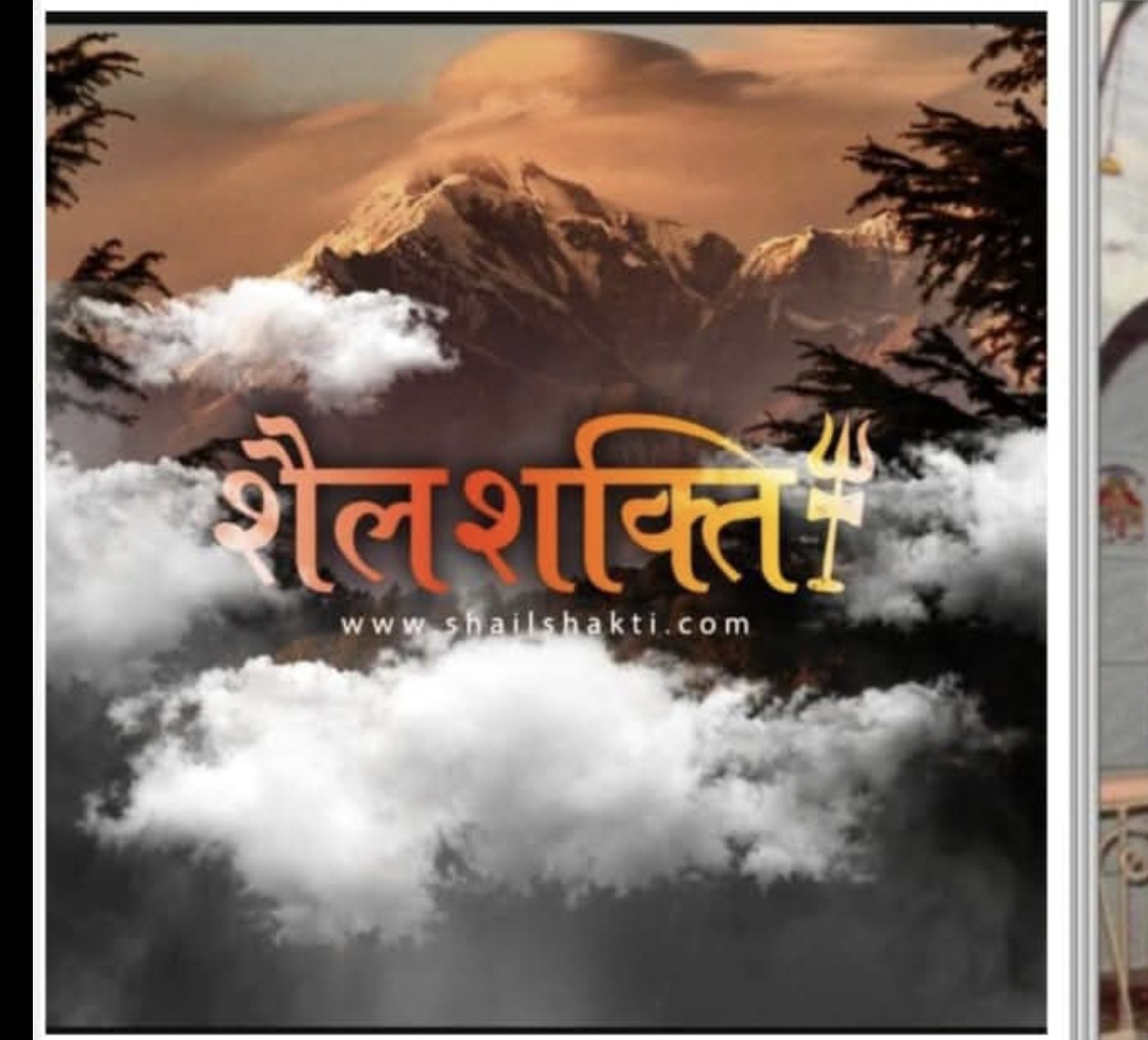गौतम बुद्ध, जिन्हें विश्व में शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से मानवता को एक ऐसा मार्ग दिखाया जो हिंसा और युद्ध से परे है। बुद्ध का दर्शन न केवल व्यक्तिगत शांति और आत्म-जागृति पर केंद्रित है, बल्कि सामाजिक और सामूहिक स्तर पर भी शांति स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करता हैं। युद्ध, जो मानव इतिहास में विनाश, दुख और विभाजन का कारण रहा है, बुद्ध के दर्शन में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया, जो उनके दर्शन का आधार बने। इन सिद्धांतों में हिंसा और युद्ध का कोई स्थान नहीं था। बुद्ध का मानना था कि सभी प्राणी सुख की खोज में हैं और दुख से मुक्ति चाहते हैं। युद्ध, जो हिंसा और विनाश का प्रतीक है, इस खोज को न केवल बाधित करता है, बल्कि दुख को और बढ़ाता है।
बुद्ध के दर्शन का मूल आधार अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि हिंसा से केवल और हिंसा जन्म लेती है। एक प्रसिद्ध धम्मपद श्लोक में बुद्ध कहते हैं:
*”न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं।*
*अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो।”*
अर्थात्, “नफरत से नफरत कभी शांत नहीं होती; नफरत को केवल प्रेम और करुणा से शांत किया जा सकता है। यह शाश्वत नियम है।” यह श्लोक बुद्ध के युद्ध के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। युद्ध, जो घृणा, क्रोध और लोभ से प्रेरित होता है, कभी भी शांति और सौहार्द का कारण नहीं बन सकता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि प्रत्येक प्राणी के भीतर बुद्धत्व की संभावना है, और इसलिए प्रत्येक जीवन मूल्यवान है। युद्ध में होने वाली हत्याएं और विनाश इस मूल्य को नष्ट करते हैं और मानवता को उसके उच्चतम लक्ष्य निरंतर शांति और जागृति से दूर ले जाते हैं।
बुद्ध ने युद्ध के कारणों को मानव मन की तृष्णा (लोभ), क्रोध और अज्ञानता में देखा। उनके अनुसार, ये तीन “विष” (लोभ, द्वेष, मोह) मानव दुख के मूल कारण हैं। युद्ध अक्सर क्षेत्रीय विस्तार, धन, शक्ति या वैचारिक मतभेदों के कारण होते हैं, जो सभी तृष्णा और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में इन मूल कारणों को समझने और उन्हें समाप्त करने पर जोर दिया।
बुद्ध के समय में कई छोटे-छोटे राज्यों के बीच युद्ध और संघर्ष आम थे। बुद्ध ने इन युद्धों को रोकने के लिए कई बार मध्यस्थता की। एक प्रसिद्ध घटना में, शाक्य और कोलिय जनजातियों के बीच रोहिणी नदी के जल विभाजन को लेकर विवाद हो गया था, जो युद्ध का रूप लेने वाला था। बुद्ध ने दोनों पक्षों को समझाया कि जल के लिए युद्ध करने से होने वाली हानि जो मानव जीवन और रिश्तों के नुकसान के रूप में होगी उस जल के मूल्य से कहीं अधिक होगी। उनकी मध्यस्थता से दोनों पक्षों ने शांति स्थापित की। यह घटना दर्शाती है कि बुद्ध युद्ध को केवल हिंसा के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि इसे मानवता के लिए एक अनावश्यक दुख के रूप में समझते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि युद्ध के बजाय संवाद, समझ और करुणा के माध्यम से समस्याओं का समाधान संभव है।
बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं था, वे सामाजिक और सामूहिक शांति के भी पक्षधर थे। उन्होंने राजाओं और शासकों को भी उपदेश दिए कि शासन का आधार धर्म (नैतिकता), करुणा और न्याय होना चाहिए। बुद्ध ने चक्रवर्ती राजा (आदर्श शासक) की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो बिना हिंसा और युद्ध के, धर्म के आधार पर शासन करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि शांति तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और करुणा हो। युद्ध अक्सर सामाजिक असमानता, अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे अपने कर्मों से समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा दें।
बौद्ध धर्म में युद्ध की नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। कुछ अन्य धर्मों या दर्शनों में “न्यायपूर्ण युद्ध” की अवधारणा हो सकती है, लेकिन बुद्ध के लिए कोई भी युद्ध न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा दुख और विनाश होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना केवल दुख को बढ़ाता है। इसके बजाय, उन्होंने करुणा, क्षमा और समझ के मार्ग को अपनाने की सलाह दी। बुद्ध के समय में, कई योद्धा और सैनिक उनके पास आकर यह प्रश्न करते थे कि युद्ध में भाग लेना उनके कर्तव्य का हिस्सा है, तो क्या यह गलत है? बुद्ध ने उन्हें समझाया कि हिंसा में भाग लेना, भले ही वह कर्तव्य के नाम पर हो, कर्म के नियमों से मुक्त नहीं है। हिंसा करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को दुख देता है, बल्कि अपने लिए भी दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने सैनिकों को सलाह दी कि वे अपने मन को शुद्ध करें और हिंसा के बजाय शांति के मार्ग को चुनें।
आज के युग में, जब विश्व युद्ध, आतंकवाद और हिंसा की चुनौतियों से जूझ रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। बुद्ध का अहिंसा और करुणा का संदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति ला सकता है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है।आधुनिक विश्व में, कई संगठन और नेता बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित होकर शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म के एक प्रमुख नेता हैं, ने बार-बार विश्व शांति के लिए अहिंसा और करुणा के महत्व पर जोर दिया है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि युद्ध और हिंसा से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इसके बजाय, संवाद, सहानुभूति और आपसी समझ के माध्यम से ही शांति संभव है।
गौतम बुद्ध ने युद्ध का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके दर्शन का मूल आधार अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव था। युद्ध, जो मानव मन की तृष्णा, क्रोध और अज्ञानता से उत्पन्न होता है, बुद्ध के लिए केवल दुख और विनाश का कारण था। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह दिखाया कि शांति का मार्ग हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समझ से होकर गुजरता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में और समाज में शांति को बढ़ावा दें। युद्ध और हिंसा के इस युग में, बुद्ध का संदेश एक प्रकाशस्तंभ की तरह है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को शुद्ध करें और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखें। बुद्ध का यह दर्शन न केवल उनके समय में, बल्कि आज और भविष्य में भी मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है।

*(संदीप सृजन-विभूति फीचर्स)*

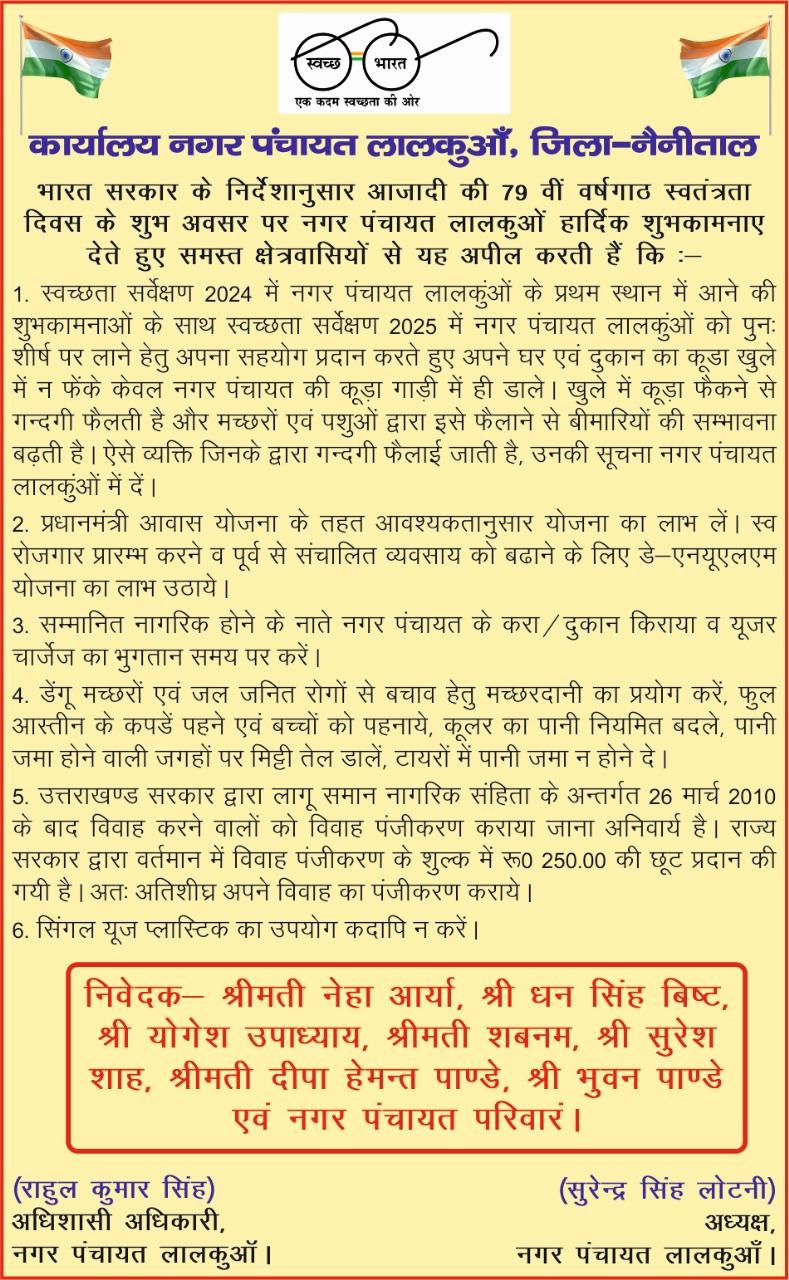
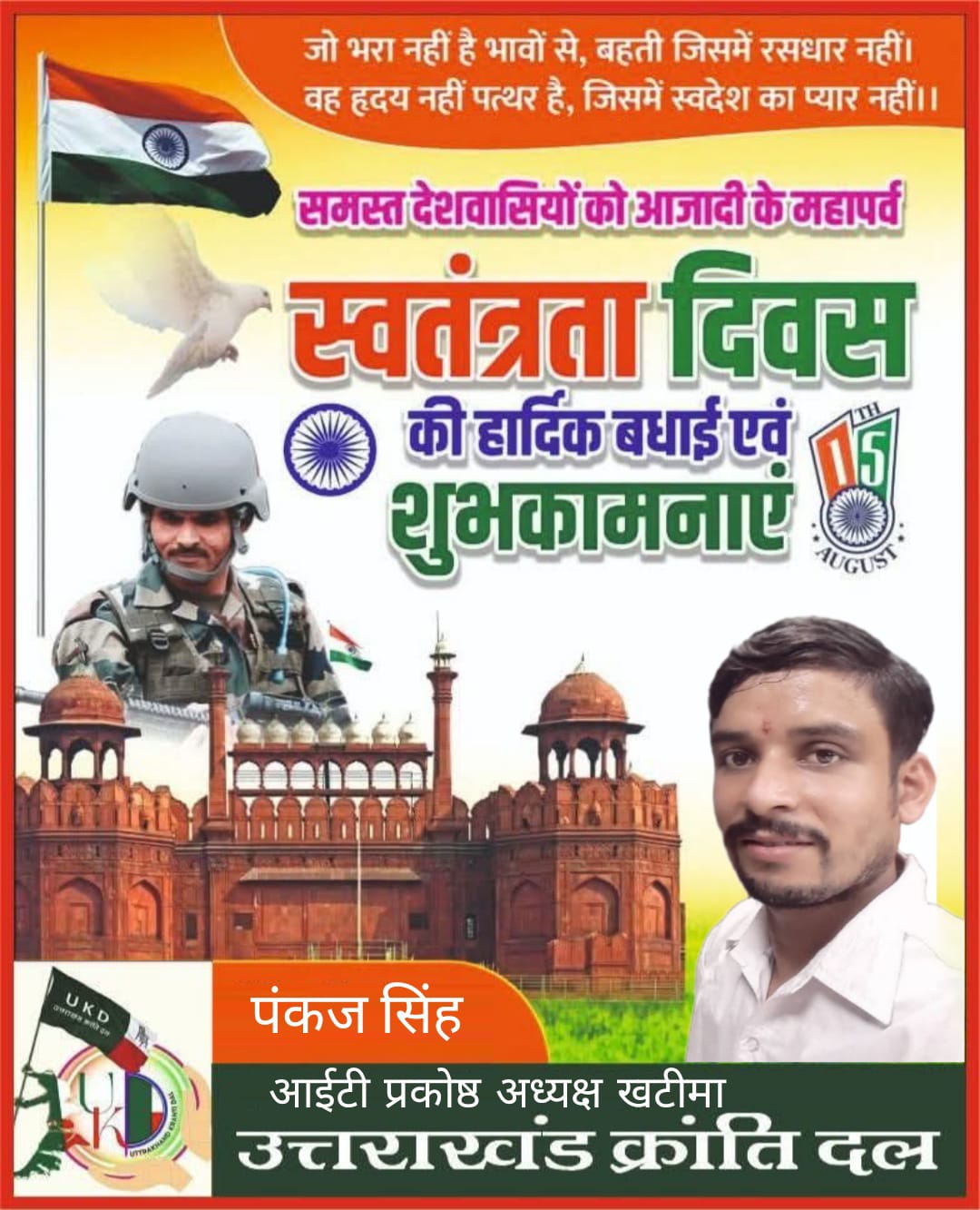
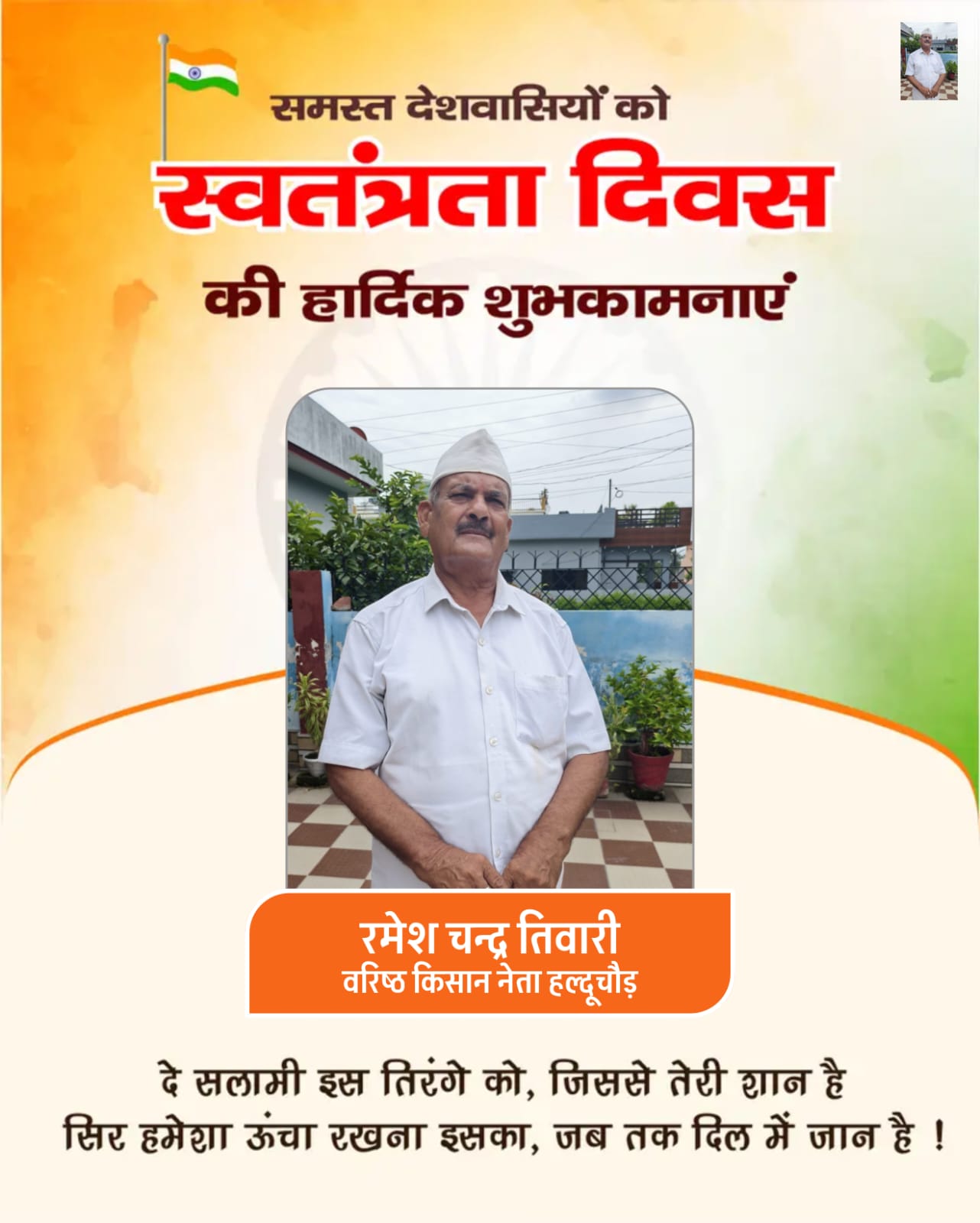
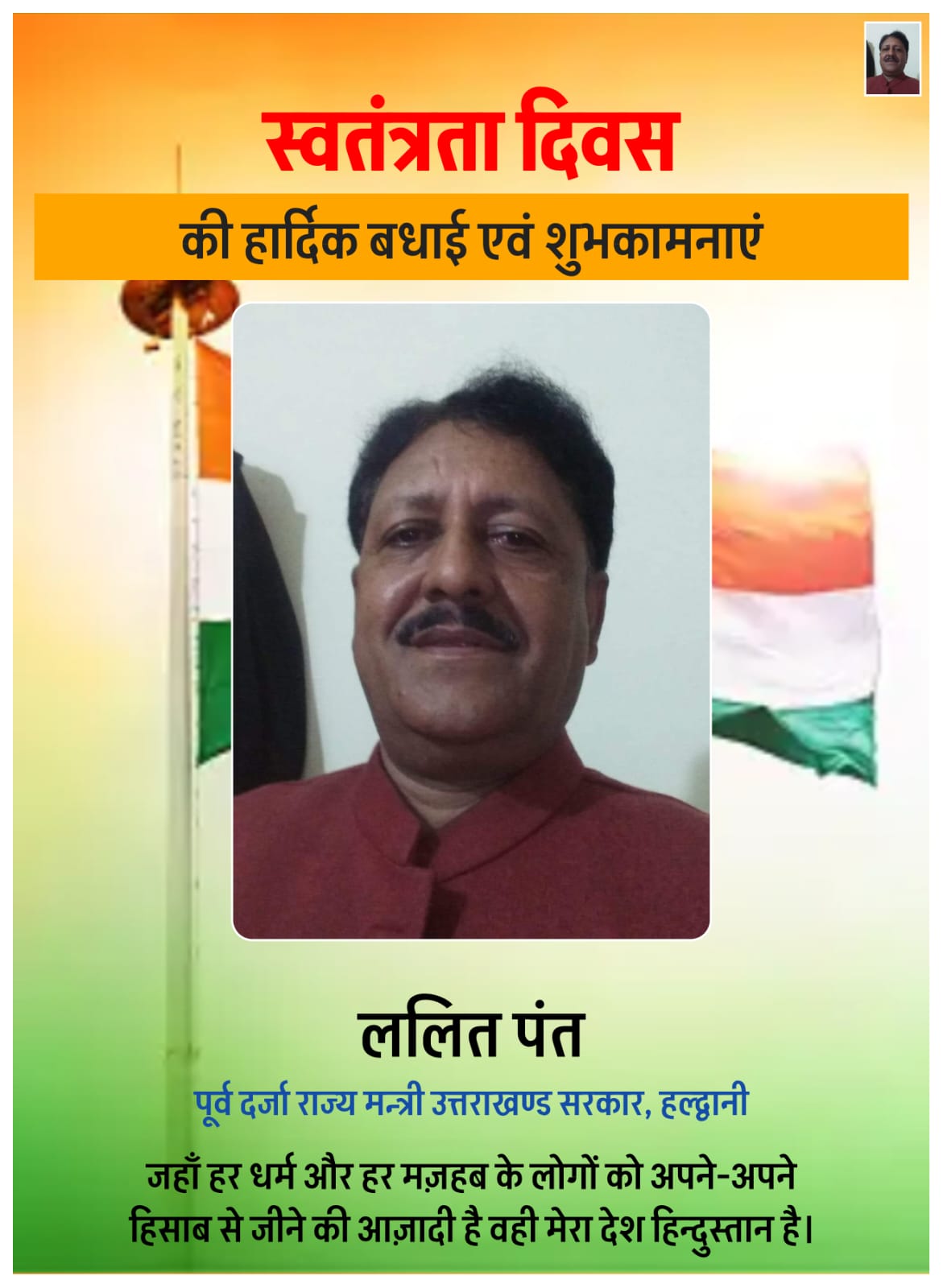
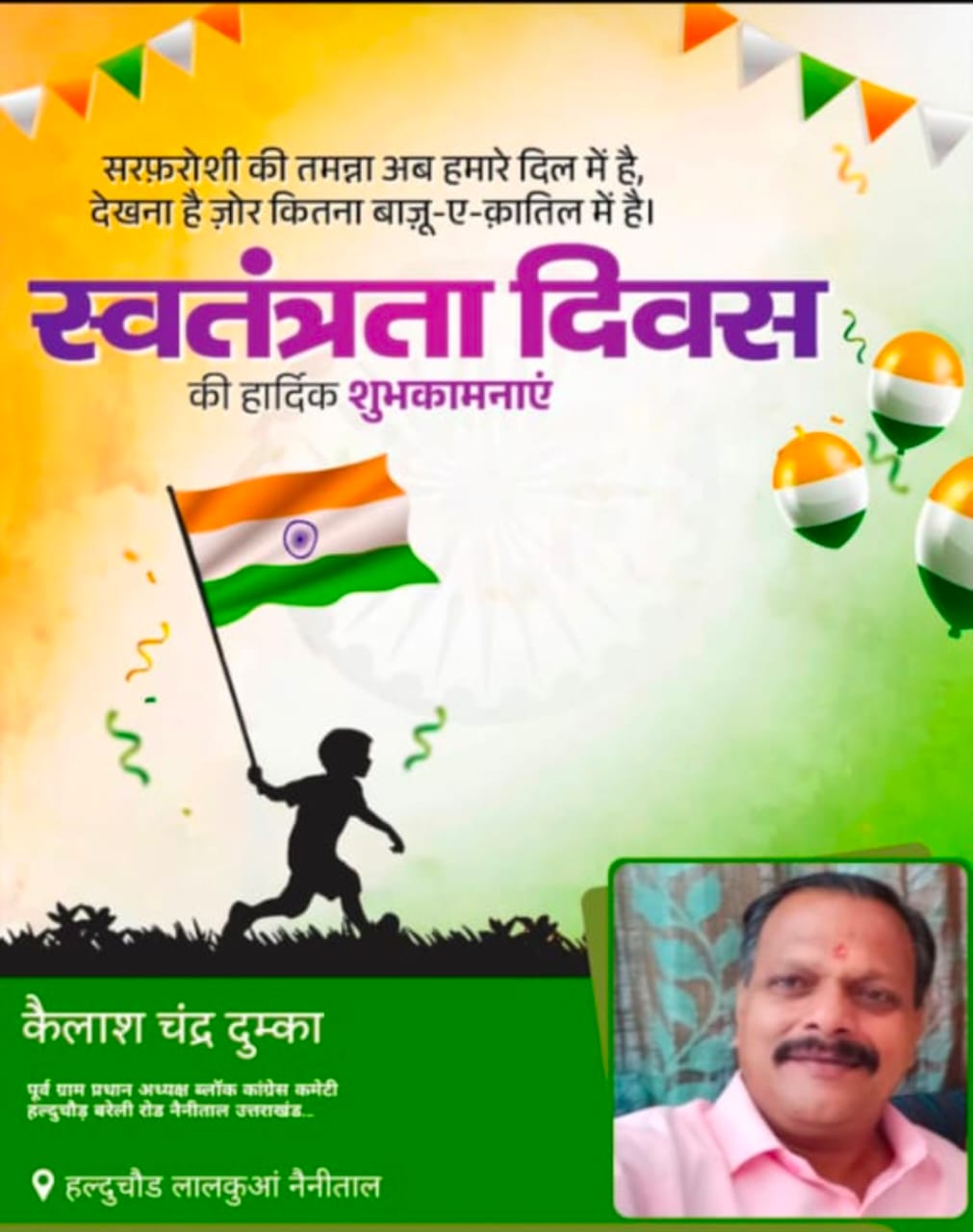
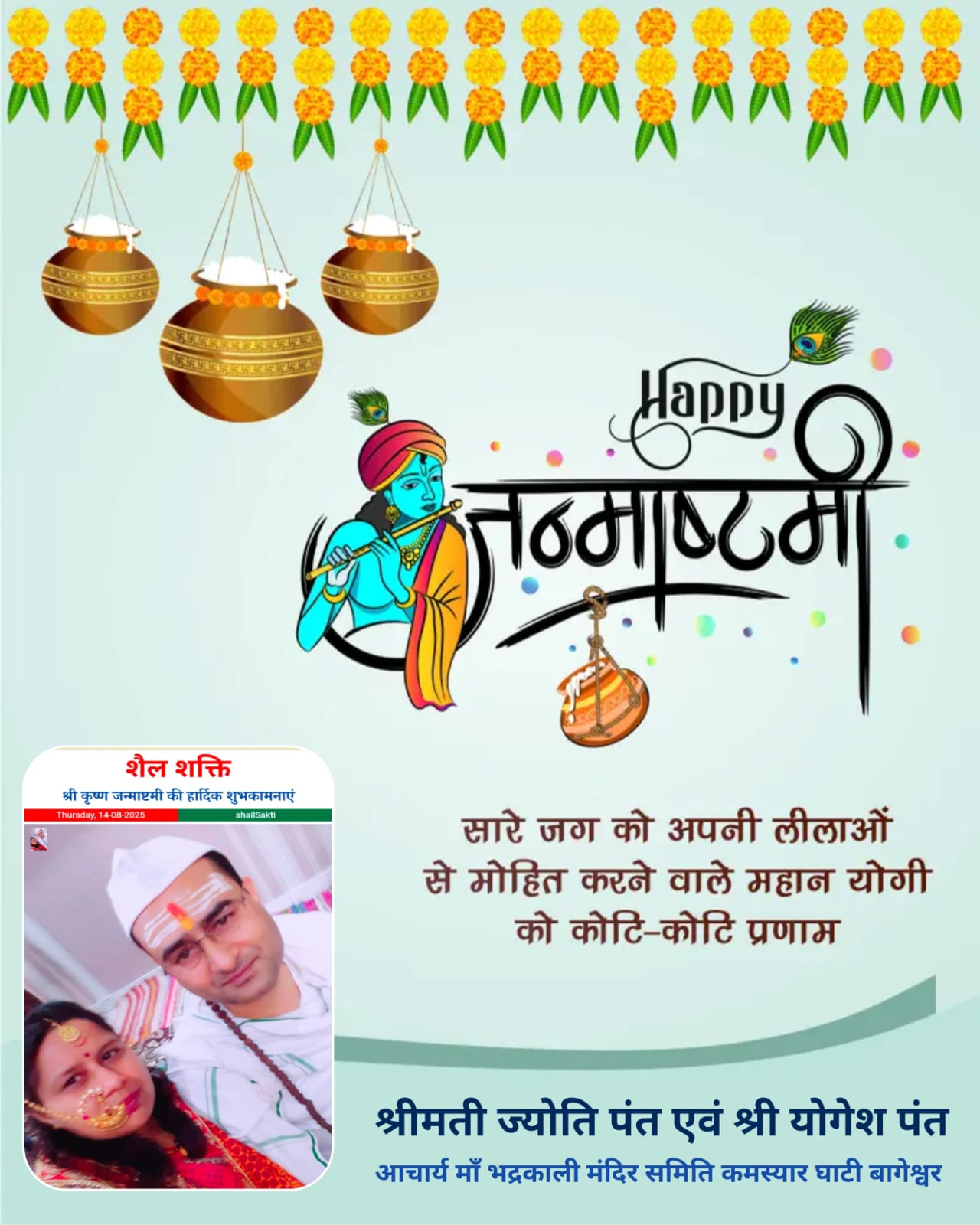
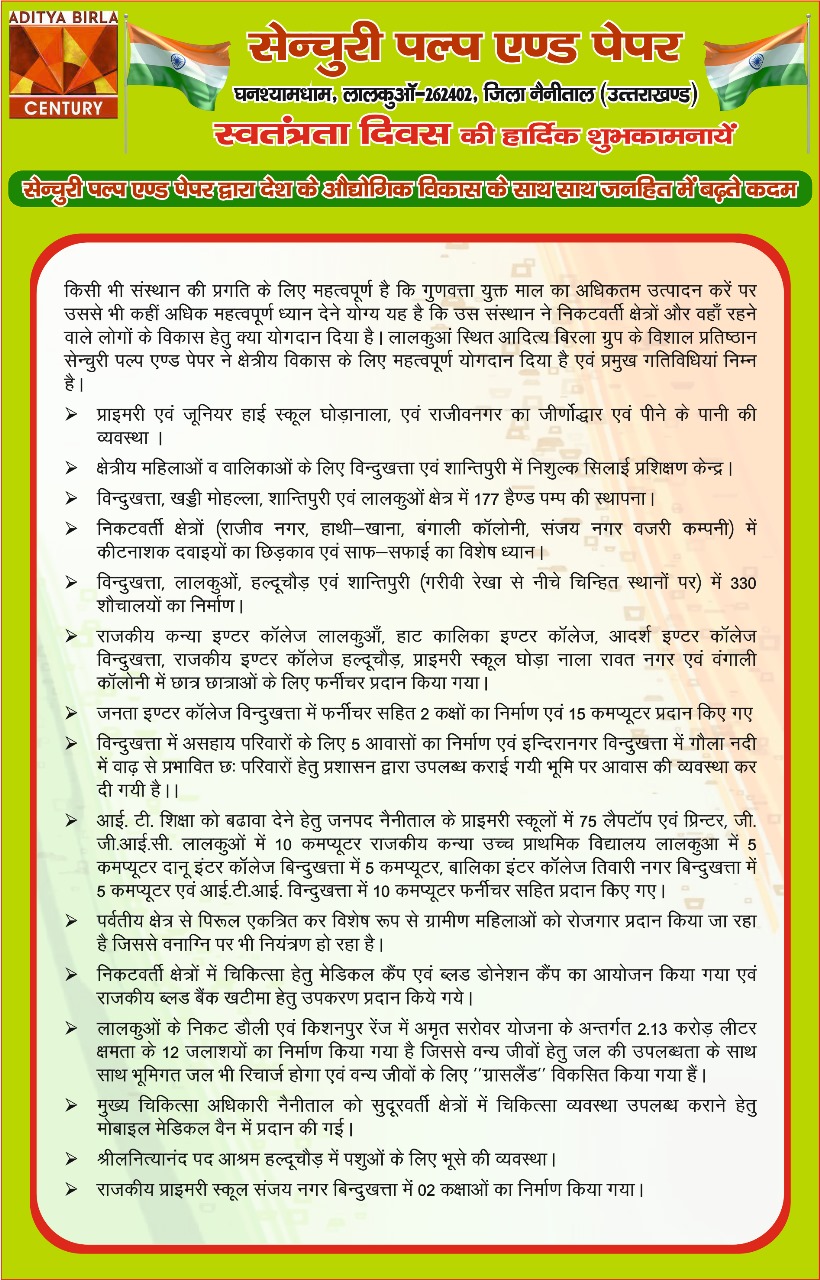



लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें